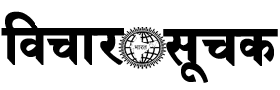साक्षात्कार: बालेंदु द्विवेदी

सवाल:एक लेखक और लोकसेवक के रूप में आपकी दो भूमिकाएं हैं।आपने किसे महत्त्व दिया और किसे इग्नोर किया या कम मान दिया?कई बार अपने जो जीवकोपार्जन के लिए जो काम करते हैं उसको इग्नोर करते हैं उसमें कटौती करते हैं चोरी करते हैं।इसी से जुडा हुआ एक सवाल और की दोनों में से इन दोनों भूमिकाओं में से आप किसको ज्यादा प्रेम करते हैं?
बालेंदु:मुझसे कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि इतने कामों के बीच आप कैसे लिख पाते हैं?समय कैसे निकाल पाते हैं।मैं उनसे कहता हूं कि शायद यह लिखना ही है जिससे इतने कामों का होना संभव कर पाता है।लिखना मुश्किल काम है।और उपन्यास जैसी विधा को साधना और भी मुश्किल।फिर रोज समय भी नहीं मिल पाता।जब मिलता है तो कोई जरूरी नहीं कि उस समय मूड और माहौल बने ही।इसके बावजूद मन में एक विचार-सरणी सदैव बहती रहती है।मैं उसमें सदैव गोते लगता रहता हूं और आनंदित होता रहता हूं।मेरे लिए दोनों काम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।बस इतना है कि एक साधन है और दूसरा साध्य।साधन को इग्नोर नहीं किया जा सकता।क्योंकि यदि साधन प्रभावित हुआ तो साध्य पर भी असर डालेगा ही।मेरे लिए दोनों सम्माननीय हैं।
सवाल:आपका पहला उपन्यास मदारीपुर जंक्शन तीन साल पहले आया था।अब वाया फुरसतगंज छपकर आया है।तब में और अब में क्या अंतर महसूस करते हैं?
बालेंदु:मदारीपुर जंक्शन को मैंने वर्ष 2011 में लिखना शुरू किया था।तब यह तय नहीं था कि क्या निकालकर आयेगा;या कुछ निकलकर आ पाएगा भी या नहीं।फिर ऐसा भी हुआ कि लगभग डेढ़ साल इस पर कुछ नहीं लिखा।वर्ष 2014 के आरंभ से 2015 के मध्य तक इसको लिखकर पूरा किया।लेकिन सवाल बड़ा था कि यह छपे कैसे?क्योंकि पूरा होने के बाद एक साल तक मेरे पास कोई प्रकाशक ही नहीं था।इसलिए इस अवधि में मैं न केवल प्रकाशक तलाशता रहा बल्कि मदारीपुर जंक्शन का पूर्व लिखा तराशता भी रहा।तब भी छपने की इतनी जल्दी नहीं थी।क्योंकि यह आत्मविश्वास था कि कुछ बेहतर रच गया है और इसे छपने के पूर्व जितना तराशा जाय उतना ही अच्छा होगा।क्योंकि एक बार जब पुस्तक पाठकों के हाथ में पहुंच जाती है;तब आप कुछ नहीं कर सकते।तब आप केवल प्रतिक्रियाओं के मूक साक्षी भर बनकर रह जाते हैं।
वाया फुरसतगंज के साथ वह कठिनाई नहीं थी।यहां चुनौती दूसरी थी।यह थी पाठकों के उम्मीदों पर खरे उतरने की चुनौती।क्योंकि जब मदारीपुर जंक्शन छपकर आया था तब कर अपना कोई पाठक वर्ग तो था नहीं..!इसने ही एक पाठक वर्ग तैयार किया।इसे पाठकों का बहुत प्यार मिला।इसलिए अबकी बार चुनौती बड़ी थी।अपनी ही खींची एक लकीर के बरक्स एक दूसरी लकीर खींच कर दिखानी थी।अबकी बार प्रकाशक भी पास में थे और लोगों की उम्मीदें आसमान पर।मैंने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बड़े इत्मीनान से कदम आगे बढ़ाए।सबसे पहले कहानी पर काम शुरू किया।कहानी ऐसी हो जिसके इर्द गिर्द व्यंग्य का वातावरण रचा जा सके।आत्ममंथन का दौर था।तभी एक दिन मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि एक गांव में कुएं से एक बकरे को निकालने के चक्कर में पिता और पुत्र दोनों अपनी जान गंवा बैठे।बस यहीं मुझे अपनी नई कहानी का प्रस्थान बिंदु मिल गया।मैंने इस कहानी को बुनने और इसके कथानक को तनिक विस्तार देने का काम शुरू किया।पहले से एकत्रित कच्चे माल को भी इसके साथ लगाना शुरू किया।धीरे-धीरे वाया फुरसतगंज की कहानी शक्ल लेने लगी। मई,2019 में जब इसका पहला ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ तो उस समय मैंने अपने एक सीनियर दोस्त को इसे दिखाया।उन्होंने इसमें कुछ छोटे छोटे करेक्शन सुझाए।फिर इसके हिसाब से कहानी के अंतिम परिच्छेद में मैंने कुछ परिवर्तन भी किया।और अब वाया फुरसतगंज आप सभी के सामने है।
सवाल: मदारीपुर जंक्शन और वाया फुरसतगंज-इन दोनों उपन्यासों में कितनी समानता है और दोनों एक दूसरे कितने भिन्न हैं..?
बालेंदु:मदारीपुर जंक्शन में गांव केंद्र में भी था और परिधि पर भी.!फिर इसका परिवेश,वातावरण,संस्कृति,भाषा बोली बनी सब कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी संस्कृति के बेहद करीब था।कहानी में समाज और राजनीति दोनों केंद्र में थे।यहां स्थानीय राजनीति के बहाने समाज की जड़ताओ पर प्रहार करने की कोशिश की गई थी।उसमें ढेर सारे विमर्श तलाशे गए थे मसलन दलित विमर्श;स्त्री विमर्श आदि।
वाया फुरसतगंज में कहानी का यह प्लाट शिफ्ट होकर इलाहाबाद और उसके आसपास की ठेठ संस्कृति हो गया है।यहां गांव तो केंद्र में है ज़रूर;लेकिन इसकी परिधि पर एक प्रकार से हमारा सारा हिन्दुस्तान ही है।वाया फुरसतगंज में मुख्यधारा की पूरी राजनीति केंद्र में है।और इसके बहाने से हमारा संपूर्ण तंत्र भी।
सवाल:आपने अपने नए उपन्यास वाया फुरसतगंज में,एक गांव के बहाने इलाहाबाद,जिसे अब प्रयागराज कहते हैं,की ठेठ संस्कृति को सामने रखा है।इलाहाबाद को केंद्र में रखने की कोई खास वजह?
बालेंदु:इलाहाबाद से मेरा गहरा लगाव रहा है।मेरी पढ़ाई वहीं से हुई है और मेरी नौकरी का भी अधिकांश वहां बीता है।इसलिए वाया फुरसतगंज एक प्रकार से इस शहर से उऋण होने का उपक्रम है।लेकिन आरंभ में वाया फुरसतगंज की रचना मेरे इतनी आसान कभी नहीं रही।मेरी मातृभाषा भोजपुरी है और इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है।फिर इसकी ठेठ अवधी बोलना अत्यंत कठिन है।ऐसे में इसे महसूस करना,इसे कागज़ पर उतारना और इसे अंत तक निभाना अपने आप में एक बड़े चैलेंज की तरह था।फिर लिखते समय निपट स्थानीय बोली और कहावतों को उनके मूल रूप में लेकर आना भी एक बड़ी चुनौती थी।शुरुआत में लगा कि मैं इसके साथ न्याय कर भी पाऊंगा या नहीं..!लेकिन एक बार जब कथानक ने रिदम पकड़ा तो फिर आत्मविश्वास आता गया।फिर तो एक समय ऐसा भी आया जब वाया फुरसतगंज कंप्लीट करने के बाद भी लंबे समय तक उसके चरित्र और संवाद मेरे जेहन में घूमते रहते थे।आज जब वाया फुरसतगंज को पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक सुखद एहसास का अनुभव होता है कि भिन्न भाषा और भिन्न संस्कृति भी किसी प्रकार से मेरी लेखनी के लिए बाधक न बन सकी।
सवाल:विधा के रूप में उपन्यास विधा का ही चयन ही क्यों?और इसके लिए भी व्यंग्यात्मक शैली ही क्यों?
बालेंदु:यह सवाल जितना आसान दीखता है उतना है नहीं।अव्वल तो यह निष्कर्ष ही गलत है कि विधाओं और शैली का चुनाव हम करते हैं।यदि ऐसा होता तो हर रचनाकार जब चाहता तो हर विधा में हाथ आजमा लेता।जिस शैली में चाहता लिख लेता।जब चाहता कहानी लिखता,जब चाहता उपन्यास लिखता और जब चाहता तो कविता और निबंध लिखने बैठ जाता..!लेकिन ऐसा होता नहीं है।क्यों विधा हमें स्वयं चुनती है।इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में ढेर सारी प्रवित्तियों और संस्कारों का हाथ होता है।ये मिलकर हमारे जिस व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं;कालांतर में वे वृत्तियां केवल उन्हीं विषयों को ग्रहण करती हैं जो उसके अनुकूल होती हैं।शैली भी बहुत कुछ वृत्ति से निर्धारित होती चलती है।शैली हमारे व्यक्तित्व का अनिवार्य अंग है;जिसे हम चाहकर भी अपने से पृथक नहीं कर सकते।अगर पृथक करने चलेंगे तो बेनकाब हो जाएंगे।क्यों तब हमारा नकाब उतर जाएगा।इसलिए जिसे हम विधाओं का चयन या शैली का अंगीकार किया जाना कहते हैं;दरअसल वह स्वतःस्फूर्त है और उसमें कोई सायास बदलाव संभव नहीं है। मैं उपन्यास इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं उपन्यास ही लिख सकता था।समय के दबावों ने मुझे ऐसा ही बनाया।इसी प्रकार मैं व्यंग्यात्मक शैली में ही लिख सकता था। क्योंकि व्यंग्य मेरी रगों का हिस्सा है,मेरे संस्कारों का हिस्सा है।मैं और व्यंग्य लगभग एक दूसरे के पर्याय हैं।
सवाल:आपके उपन्यासों में चरित्रों का गठन बहुत मजबूत दीखता है।चाहें मदारीपुर जंक्शन के छेदी बाबू हों,बैरागी बाबू हों, वैद्यजी हों या फिर चइता या मेघिया..!वाया फुरसतगंज में भी जोखन सिंह,बच्चा तिवारी,जबर सिंह,झारखंडे राय,पोलो गुरू,पाखंडी शर्मा आदि के चरित्र बहुत प्रभावशाली बन पड़े हैं।इनका गुम्फन बहुत बारीक है और कथावस्तु की गति बनाए रखने में बहुत सहायक है।आपने चरित्र निर्माण की यह शैली कहां से ग्रहण की या इसे कैसे विकसित किया?
बालेंदु:यह सही है कि मेरे पाठकों को मेरे रचे चरित्रों में आनंद आने लगा है।और यह भी सच है कि जब मैं अपने किसी पात्र का गठन करता हूं तो उसके निर्माण के समय स्वयं भी आनंदित आह्लादित होता चलता हूं।जब लेखक और पाठक के बीच संवेदना का यह ऐक्य होता है तभी आनंद द्विगुणित होता है।लेकिन मेरे लिए यह बता पाना शायद बहुत कठिन है कि यह अंदाज़ मुझे कहां से हासिल हुआ या मैंने इसे कहां से सायास ग्रहण किया।जहां तक मेरी कुंद जेहनी मुझे अवगत कराती है तो यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कहीं न कहीं ये चरित्र मेरे आसपास के चरित्र हैं;वहां से निकलते हैं जहां मैं पैदा हुआ; पला बढ़ा अथवा जहां मैं लंबे समय तक रहता आया हूं।फिर हर एक चरित्र में कई कई चरित्र समाए हुए हैं।अपने आसपास के कई चरित्रों को मिलाकर एक चरित्र बनाता हूं और उसमें अपनी कल्पना से कुछ जोड़ता भी हूं।फिर कोशिश यह भी करता हूं कि उसकी हारमोनी मुख्य कथा के साथ बनी रहे।कहीं से भी कुछ असंगत न लगे;जोड़ा हुआ या चिपकाया हुआ न लगे।फिर यह भी देखना होता है कि कहीं से कुछ दूसरे से मिलता जुलता न लगे।कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पात्र को गढ़ने की प्रक्रिया में ऐसा लगने लगता है कि यह तो फलां उपन्यास के फलां पात्र की तरह होता जा रहा है।ऐसे में उसे या तो ड्रॉप करना पड़ता है या उसमें कुछ आंशिक संशोधन करना पड़ता है।ताकि नकल का ठप्पा न लगे।
सवाल:आपके उपन्यासों में प्रयुक्त लोकगीत,कहावतें और लोकोक्तियां इसकी जान हैं।ये उस समाज के संस्कार को समझने का एक बड़ा माध्यम बन सकती हैं।आप अपने उपन्यासों में इनका विधान कैसे करते हैं?
बालेंदु:किसी भी समाज को समझना है तो उसमें प्रचलित लोकगीत,लोककथाओं और लोकोक्तियों का अध्ययन कीजिए; उसमें आपको वहां का पूरा का पूरा समाजशास्त्र दिख जाएगा।उत्तर भारत के समाज में इनका बड़ा महत्त्व है।मैं जिस माटी में पैदा हुआ और पला बढ़ा; वहां के समाज में बात-बात में लोकोक्तियों और लोककथाओं का प्रयोग होता है।किस्से-कहानियां इतनी कि इन्हें सुनकर बहुत कुछ सीखा जा सके।मैं सालों-साल इनके संग्रह में लगा रहता हूं।जब भी अपने गांव जाता हूं तो ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना चाहता हूं जिनके पास वाचिक परम्परा से प्राप्त किस्सों कहावतों का एक वृहद संसार है।मैं उसे नोट करता चलता हूं।क्योंकि जानता हूं कि यदि इसे किसी बहाने से कलमबद्ध नहीं किया गया तो एक समय के बाद इसे सुनाने वाला भी कोई नहीं रह जाएगा।और तब ये चीज़ें पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी।इसलिए जब मैं कुछ लिखने चलता हूं तो मेरे पास किस्सों की भरमार होती है।फिर एक बड़े किस्से के भीतर छोटे छोटे अनसुने किस्से या कम सुने गए किस्सों को पिरोता चलता हूं।यह मेरी किस्सागोई का अभिन्न हिस्सा है।और मुझे ऐसा करने में मुझे आनंद आता है।कदाचित इसीलिए आप देखेंगे कि चाहें मदारीपुर जंक्शन हो या वाया फुरसतगंज;दोनों में लोकोक्तियों और लोककथाओं का एक भरा पूरा संसार है।
सवाल:स्वाभाविक सी बात है कि एक रचनाकार जब कोई कहानी या उपन्यास लिखता है तो उसकी रचना में उसकी निजता झलकती है।लेकिन इसका मिश्रण बहुत बारीक होना चाहिए अन्यथा कहानी या उपन्यास,आत्मकथा बन जाएगा।आपके उपन्यासों में आपका ‘स्व’ कितना समाहित हुआ है ?
बालेंदु: हर रचनाकार स्वयं को ही लिखता है।और मैं तो कहता हूं एक ही चीज को बार-बार लिखता है।इसलिए उसका जो कुछ भी लिखा हुआ है वह उसका स्व ही होता है।बस वह चालकी इतनी करता है कि वह एक चालाक ग्वाले की तरह दूध में तनिक पानी मिला देता है।इस मिश्रण को केवल वह जानता है;ग्राहक नहीं।ऐसा ही एक रचनाकार अपनी कल्पनाशीलता के साथ करता है।वह अपने और हमारे आसपास से ही चीज़ें उठाता है और उसमें अपनी कल्पना के मिश्रण से कुछ ऐसा रचता है कि सब कुछ नया लगने लगता है।यह भी लगता है कि ‘अरे..!ऐसा तो मैंने भी देखा है।’ ‘ऐसा तो मैंने भी सुना है।’ यहां केवल रचनाकार की अपनी कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता काम आती है।और हर रचनाकार की यह कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता उसका अपना निजी हथियार है;जिसके बिना कुछ भी नहीं लिखा जा सकता।लेकिन इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोई भी रचनाकार ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकता जिसे उसने कभी देखा सुना या भोगा न हो;या उसे संवेदना के धरातल पर उतरकर गहराई से महसूस न किया हो।यदि वह कुछ ऐसा रचना चाहे भी,जो इसके इतर हो तो उसमें वह वास्तविकता न आ पाएगी।और अगर वास्तविकता नहीं आएगी तो पाठक उसकी कथा के साथ साम्य या ऐक्य नहीं बिठा पाएगा।मेरे लेखन में भी मेरा स्व है।मदारीपुर जंक्शन की कहानी का तो प्लॉट ही मैंने वह रखा है जहां मैं पैदा हुआ और पला-बढ़ा।वाया फुरसतगंज में भी कल्पना है लेकिन यथार्थ मेरा अपना देखा और भोगा हुआ है।इसी तरह से मेरे नाटक में खदेरू और मुनिया की कहानी मेरे अपने ही एक नौकर रमालू और उसकी पत्नी की असल कहानी है।उसके जीवन से बहुत मिलती-जुलती है।बहुत सारे लोग उसमें मुंशी प्रेमचंद के ‘कफ़न’ कहानी का अक्स देखते हैं।जबकि वास्तविकता यह है कि यह कहानी मेरा देखा हुआ यथार्थ है।कहना यह कि बिना ‘स्व’ को शामिल किए कुछ भी नहीं रचा जा सकता।कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता इसके गठन को बाकियों से अलगाती है।
सवाल:आपने नाटक में भी हाथ आजमाया है.’मृत्युभोज’ आपका लोकप्रिय नाटक है.लेकिन आपने नाटकों पर ज़्यादा काम नहीं किया।ऐसा क्यों?
बालेंदु:देखिए..! मैं कोई नाटककार नहीं हूं।लेकिन दो उपन्यासों और एक नाटक को रचने के बाद यह समझ में आया कि बिना नाटकीयता के तो न तो कहानी बन सकती है और न उपन्यास।नाटक में तो यह है ही।पहली बार जब मदारीपुर जंक्शन पर नाट्य-मंचन शुरू हुए तब मुझे लगा कि मेरे लेखन में नाटकीयता एक प्रबल तत्त्व है।या इसे यूं कहूं कि मेरे पास ऐसा एक हथियार था;इसका भान मुझे तब हुआ।मृत्युभोज मेरी एक कहानी थी;जो निकट पत्रिका में छपी थी।जब यह छपकर आई तो मैंने इसे कुछ लोगों को भेजा।नौ परिच्छेद की कहानी थी यह।उसी समय यह आइडिया दिमाग में आया कि इसे नाटक का रूप भी दिया जा सकता है।फिर इसे संशोधित करना शुरू किया।और अंत में यह तेरह परिच्छेद में बनकर तैयार हुई।इसमें कुछ पारंपरिक गीत जोड़े जो स्त्री के विवाह,विदाई और दुखद अंत पर गाए जाते हैं।नौ पेज की कहानी 64 पेज में बनकर तैयार हुई।
जहां तक नाटकों पर काम करने या न करने का सवाल है;अभी मुझे इस क्षेत्र में काम करना बाकी है।आजकल स्वतंत्र नाटक बहुत कम लिखे जा रहे हैं।जो लिखे भिंजा रहे हैं वे विशुद्ध साहित्यिक नहीं हैं;केवल रंगमंच के लिए लिखे गए हैं।ऐसे नाटक दीर्घजीवी नहीं होते।मेरी कोशिह है कि प्रासंगिक और दीर्घजीवी प्रभाव वाले साहित्यिक नाटक लिखे जाएं।लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।सही विषयवस्तु की तलाश हमेशा रहती है।सबसे बड़ी चीज कि इंसान की ही तरह हर रचना के जन्म का भी समय पूर्वनिर्धारित है।लेखक के मस्तिष्क में उसका पुंसवन तो हो जाता है;लेकिन वह कब आकार लेगी,इसे स्वयं लेखक भी नहीं जानता।रचना अपना स्वरूप और अपना भविष्य लेकर स्वयं प्रस्फुटित होती है।
सवाल:कई बार लेखक को नहीं पता होता है कि वह जो लिख रहा है वो कितनी बड़ी रचना है।क्या यह सोचकर भी कोई रचना होगी कि यह अपने समय की सर्वश्रेष्ठ रचना है ?
बालेंदु:देखिए..!आजकल साहित्य में सर्वश्रेष्ठता की लड़ाई चल रही है।हर कोई सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है।उसे इसी जीवन में बल्कि साल-दो साल में ही अमर कथाकार बन जाना है;चाहें इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े।सोशल मीडिया ने इसके लिए सबसे माकूल मंच प्रदान किया है।यहां सबने सबसे अपने-अपने गैंग बना रखे हैं।यह साहित्य का गैंगवार काल चल रहा है।कोई नया लेखक मार्केट में आया नहीं कि हमले शुरू..!यहां एक की श्रेष्ठता दूसरे को कमतर बताने और उसे नीचा दिखाने पर टिकी हुई है।पोसुआ समीक्षकों का एक अलंबरदार ऐसे लेखकों के समर्थन में मुंह में पिपिहरी दबाए खड़ा है।कुछ छपा नहीं कि सम्मान में धुन चालू..!दरबारी कविता तो सुनी थी;अब दरबारी समीक्षा का दौर है।लेखक को शीघ्र ही अमरता हासिल कर लेनी है-जीते जी।वेदांत में जिसे ‘सदेह मोक्ष’ कहा गया है कुछ वैसी ही स्थिति।
ऐसा नहीं है कि साहित्य में गुटबंदी या खेमेबंदी पहली बार हो रही है।लेकिन इसके पहले जो गुट बनते थे उनकी एक वैचारिक आधारभूमि हुआ करती थी।जो आक्रमण होते थे उसमें भी एक मर्यादा हुआ करती थी।निराला भी इस आक्रमण के शिकार हुए और उनकी तरह और भी बहुतेरे..!लेकिन भाषा का स्खलन कभी ऐसा नहीं हुआ;जैसा कि आज हो रहा है।छद्म साहित्यकारों की एक लंबी फौज खड़ी हो गई है जिसने साहित्य के असल स्वरूप को वैसे ही आच्छादित कर लिया है जैसे बादल,सूर्य को ढंक लेता है।ऐसे में श्रेष्ठ रचना की बात कौन करे और कौन सुने..!सबकी अपनी-अपनी डफली है और अपना-अपना राग है।इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी रचना की श्रेष्ठता आने वाला समय तय करता है।और इसके लिए हर लेखक के पास अपना एक सुरुचिसंपन्न पाठक वर्ग होना चाहिए।सभी को यह सोचना चाहिए कि वह साहित्य का सेवक है।इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।
सवाल:आज साहित्य के नए माध्यम आ गए हैं.आज ई बुक्स हैं।किंडल एडीशनस किताबों के आ गए हैं।कहा जाने लगा है कि अब किताबें उस रूप में हमें नहीं मिलेंगी पढ़ने को जिस रूप में हम परम्परा में पढ़ते आये हैं।आपको क्या लगता है कि भविष्य में साहित्य क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही दिखेगा या आज जैसी स्थिति ही रहेगी या कि फिर सुनहरे दिन लौटेंगे और पुस्तकें लाखों की संख्या में छपेंगी और करोड़ों पाठक होंगे ?
बालेंदु:माध्यम चाहें जितने आ जाएं;लेकिन किताब को पढ़ने का जो आनंद है वे ये माध्यम कदापि नहीं दे सकते।इन माध्यमों से विस्तार हुआ है;तेजी आई है।लेकिन ये पुस्तकों के स्थानापन्न नहीं हो सकते। थूक लगाकर पन्ने पलटते का जो सुख है वह स्वर्ग के वैभव से कम मोहक नहीं है।इसे कोई ई बुक कैसे दे सकता है।इसलिए मैं तो कहता हूं कि जब तक कागज़ का अस्तित्व बना रहेगा, किताबों का क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला..!!