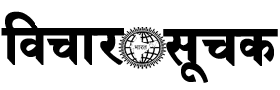इंसाफ जालिमों की हिफाजत में जायेगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जायेगा?

शीतला सिंह
पाठक अवगत हैं, केन्द्रीय जांच ब्यूरो श्सीबीआईश् की विशेष अदालत ने अयोध्या में छरू दिसम्बर, 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया है। यह तब है जब सर्वोच्च न्यायालय से लेकर लिब्राहन आयोग तक ने अपने निर्णयों और रिपोर्टों में उक्त ध्वंस को राष्ट्रीय शर्म के साथ आपराधिक और दण्डनीय कार्य कह रखा है। विशेष अदालत की मानें तो देश की जांच एजेंसियों में सबसे प्रतिष्ठित सीबीआई, जिसे ध्वंस के मामले की जांच सौंपी गई थी, उसके पीछे की साजिश के असंदिग्ध सबूत नहीं पेश कर पाई। भले ही वह कृत्य दिनदहाड़े, पुलिस-प्रशासन और कानून के रक्षकों की उपस्थिति में हुआ था। ऐसे में क्या आश्चर्य कि अब कई बार यह पूछने का भी मन होता है कि क्या बाबरी मस्जिद नाम की कोई इमारत विद्यमान भी थी, जिसे ढहाये जाने के बाद जांच का प्रसंग बनाया गया? विडम्बना देखिये- गांव-गांव और गली-गली, यहां तक कि संवाद माध्यमों में बयान देकर भी, खुद को उक्त ध्वंस में शामिल बताने और उसका जिम्मा लेने वाले आज भी विद्यमान हैं। वे 1992 जितनी ही तुर्शी और तेजी के साथ वाचाल भी हैं। लेकिन जब अदालत में पेश अभियुक्त कहें कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है, ध्वंस में उनकी कोई भूमिका नहीं है और अदालत को लगे कि सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जुटाये गये सबूत विश्वसनीय नहीं हैं तो भला कानून उन्हें कैसे दंडित कर सकता है? हम जानते हैं कि अतीत में सत्ता या सरकार की कल्पना समाज में व्यवस्था निर्धारण के लिए उसे आवश्यक मानकर की गई और दुनिया के विभिन्न भागों में इसके अलग-अलग प्रयोग हुए। पहले उस पर बलशाली लोगों का कब्जा हुआ। वे सत्तासीन हुए तो उनकी इच्छाओं और निर्देशों को ही कानून माना जाने लगा और उनके विपरीत आचरण करने वाले निर्धारित दण्ड के भागी होने लगेे। श्राजा कहे सो न्याव, पासा पड़े सो दांवश् की मान्यता स्थापित हो गई। यानी हर हाल में राजा की इच्छा ही सर्वोच्च और जिसे दंडित किया जा रहा है, वह दोषी और अपराधी। राजा या राजा को प्रभावित कर सकने वालों को शूद्रों को पूजा या तपस्या का अधिकार देना अनुचित लगा तो इस अधिकार का श्अनधिकारश् इस्तेमाल करने वाले शूद्र शम्बूक की हत्या से ही ब्राह्मण के बेटे को पुनर्जीवन मिलने का वितान रचना भी अनुचित नहीं रह गया। महिलाओं को तो सब तरह के दोषों की खान ही मान लिया गया और उनकी स्वतंत्रता की जरूरत ही नकार दी गई।
लेकिन समय के साथ इन सबके विरुद्ध असंतोष भी उभरे, जिन्होंने अलग-अलग युगों और कालों में उनकी विसंगतियों से मुक्ति के अलग-अलग ढंग के प्रयोगों को जन्म दिया। लोकतंत्र आया तो राजा के आदेश पर लोकेच्छा को तरजीह दी जाने लगी और उसे सुनिश्चित करने के लिए नई संस्थाओं का भी जन्म हुआ। फि र भी विडम्बनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हो पाईं। कारण यह कि जिस व्यवस्था को लोकतंत्र कहा गया है उसमें कम से कम हमारे देश में अभी भी सकल जनसंख्या का केवल 9 प्रतिशत ही भागीदार है। ऐसे में वास्तविक लोकेच्छाएं भला क्योंकर सामने आ और सम्मान पा सकती हैं? बहरहाल, बाबरी मस्जिद विध्वंस पर लौटें तो स्वतंत्र भारत में इसको लेकर विवाद का जन्म भले ही 22-23 दिसम्बर, 1949 को उसमें मूर्तियां रखे जाने के साथ शुरू हुआ और उसके स्वामित्व के फैसले का दायित्व न्यायालय को सौंपा गया, लेकिन जब इस विवाद को श्भये प्रकट कृपालाश् के रूप में उभारा गया हो तो उनके विरुद्ध स्वतंत्र चिंतन, विचार और निर्णय क्योंकर संभव होता? भले ही उसके स्वामित्व का फैसला करने वाला सर्वोच्च न्यायालय यह मानता हो कि उसमें मूर्तियां रखकर उस पर कब्जा करना और बाद में ध्वंस अनुचित था। भले ही पहले अदालतों में जो मामले गये हों, उनमें रामलला विराजमान का जन्मस्थल अन्यत्र बताया गया हो।
हद यह कि इस मामले में आस्था-आस्था की रट लगाने वाले आस्थावादी इस बात के लिए भी तैयार नहीं थे कि स्कन्द पुराण में जहां राम का जन्मस्थल बताया गया है, सदाशयता से उसे ही मान लिया जाये। यदि उनके द्वारा उसे आधार मान लिया जाता तो सारा विवाद किसी हिंसा और अव्यवस्था के बगैर समाप्त हो सकता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि न्यायालय भले ही कहे कि किसी हिन्दू मन्दिर को गिराकर बाबरी मस्जिद बनाने की तोहमत जांच आख्याओं और साक्ष्यों से सिद्ध नहीं होती, न्यायालय के आदेश के माध्यम से ही रामलला वहां साधिकार काबिज हो गये हैं। विवाद के वक्त जिन संस्थाओं के जन्म की कल्पना तक नहीं थी, रामलला के बहाने उन्हें ही स्वामी की प्रतिष्ठा दे दी गई है तो इसका विरोध करने वाले अनास्थावादी कहे जा रहे हैं। याद कीजिए, गत पांच अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भव्य राममन्दिर निर्माण के लिए भूमिपूजन के समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने सगर्व बताया था कि 1986 में बाबरी मस्जिद में बन्द ताले खोले जाने के बाद उनके संगठन के तत्कालीन सरसंघचालक बालासाहेब देवरस ने अयोध्यावासियों द्वारा सर्वानुमति से स्वीकार मन्दिर निर्माण के प्रस्ताव को, मन्दिर के लिए आन्दोलन करने वाले नेताओं का एक बड़ा सम्मानित वर्ग भी जिसका स्वागत कर रहा था, मानने से क्यों इन्कार कर दिया था? इसलिए कि उनके अनुसार इस हेतु उपयुक्त वातावरण 25-30 साल बाद बनना था।
तब उनका कहना था कि हम राममन्दिर के लिए आन्दोलन राजनीति के अस्त्र के रूप में दिल्ली की सत्ता पर कब्जे के लिए कर रहे हैं, इसलिए राममंदिर की ऐसी रचना और निर्माण उन्हें स्वीकार्य नहीं है। साफ है कि भागवत मानते हैं कि अब, जब भाजपा अपने बूते देश की सत्ता में है, अयोध्या ही नहीं, देश में कहीं भी मंदिर बनाने के योग्य वातावरण बन गया है। ऐसे में बाबरी मस्जिद ध्वंस के सभी आरोपियों को सम्मानित ढंग से बरी कर दिये जाने के बाद भी यह सवाल अपनी जगह है और उसे जवाब की पहले से ज्यादा दरकार है कि ध्वंस के फैसले में उनकी जमात में किसी को कोई दोष दिखता है क्या? अगर नहीं तो पहली आवश्यकता तो इस सोच में परिवर्तन की है और मस्तिष्क शुद्धि ही इसका एकमात्र विकल्प है।अब यह तो कोई बताने की बात भी नहीं है कि छरू दिसम्बर, 1992 के दिन के पहले से ही उस स्थल पर भीड़ किसने जुटाई थी और उसे जुटाने का निश्चय कब और कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को तो, जिन्हें बाबरी मस्जिद को बचाने का सर्वोच्च न्यायालय से किया गया वादा न निभाने के लिए उसकी अवमानना में एक दिन की सजा हो चुकी है, यह स्वीकारने में भी संकोच नहीं है कि उक्त ध्वंस न हुआ होता तो सर्वोच्च न्यायालय स्वामित्व के विवाद में रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला कैसे देता? ज्ञातव्य है कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद में भी कह रखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक विवादित ढांचे की हर हाल में रक्षा की जायेगी।
अब वे कम से कम इतना तो ठीक कह ही रहे हैं कि छ: दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद का कोई भी हिस्सा बच गया होता तो न्यायालय को उसके भविष्य की व्यवस्था का निर्णय भी करना ही होता। साफ कहें तो भये प्रकट कृपाला से लेकर आज तक इस सम्बन्ध में एक पक्ष द्वारा जो भी आन्दोलन और निर्णय किये गये हैं, उसके पीछे मुख्य तत्व यही रहा है कि वह न्याय उसे ही मानेगा, जिससे उसके हित सधेंगे। अब उसकी समर्थक सरकारें होने पर भी मुख्य निर्णायक तत्व का निर्धारण इस आधार पर ही होता है कि वह उसका जनसमर्थन घटाने वाला होगा या बढ़ाने वाला? ऐसे में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा ध्वंस के मामले में दिये गये ताजा निर्णय में ही विसंगतियां ढूंढते रहना उचित नहीं हैं। सोचिये जरा कि बाबरी मस्जिद के तीन गुम्बदों के बीच रामलला का प्राकट्य क्योंकर संभव हुआ और ध्वंस के बाद बाबरीमस्जिद के मलबे पर बना अस्थायी मंदिर आखिर किसकी देन थी? फैजाबाद के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तो अपनी पुस्तक में बाकायदा लिखत-पढ़त में दावा करते हैं कि ध्वंस के दूसरे दिन जब वे मौके पर गये तो जो मंदिर बना रहे थे, उन्होंने उन्हें सैल्यूट किया, क्योंकि वे वास्तव में पुलिस के सिपाही थे। इन सिपाहियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से, जो उनके इस कृत्य को अनुशासनहीनता मानकर उन्हें सजा दे सकते थे, निडर होकर कह दिया था कि कल तो हम सरकारी दायित्व निभा रहे थे, आज धार्मिक दायित्व निभा रहे हैं तो इसमें क्या दोष है? इसमें विसंगति देखने वाले हमारी आस्थाओं के दुश्मन होने के नाते अस्वीकार्य हैं।
कफ्र्यू के कारण जब अयोध्या में कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा तो अस्थायी मन्दिर निर्माण के लिए कार्यकर्ता या कारसेवक न मिल पायें तो यह भी तो हमारी आस्थाओं के विपरीत और अनुचित ही होगा। यहां यह भी याद किया जा सकता है कि ध्वंस के पहले 27 नवम्बर को ही तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने पीवी नरसिंहराव सरकार को चेता दिया था कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस निश्चित है और सरकार उसकी रक्षा नहीं कर पायेगी। इसकी चर्चा तत्कालीन गृह सचिव भी अपनी नयी प्रकाशित जीवनी में कर चुके हैं। अब अगर ध्वंस से पहले ही एक केन्द्रीय मंत्री को पता था कि बाबरी मस्जिद की रक्षा नहीं हो पायेगी तो उसके पीछे निश्चित कारण रहे होंगे। फिर भी पिंजरे का तोता कही जाने वाली सीबीआई अदालत के सामने अपना पक्ष रखती हुई उन कारणों को उजागर नहीं पाई तो जो फैसला हुआ, उसके लिए हम अदालत को ही दोषी क्यों ठहरायें? अलबत्ता, लोकप्रिय शायर राहत इंदौरी के शब्द उधार लें तो कहना होगा कि इस फैसले से सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हुआ है कि इंसाफ जालिमों की हिफाजत में जायेगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जायेगा।