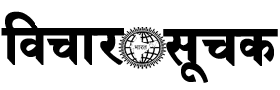सबसे खास खुफिया क्लब ‘फाइव आइज़’ में शामिल होने जा रहा है भारत?

वाशिंगटन. कैरेबियन सागर से लगभग 20 हजार मीटर ऊपर, हवाना के पश्चिम में लॉस पलासियोस के चावल के खेतों पर एक तकनीकी देवता की अचंभित आंख नजर गड़ाए थी. 14 अक्टूबर, 1962 को U2 स्पाईक्राफ्ट के Hycon 73B कैमरे से ली गई तस्वीरों में सोवियत मिलिट्री का एक काफिला सड़क से गुजरते हुए रिकॉर्ड किया गया था. इसके बाद वाशिंगटन शहर स्थित स्टुअर्ट बिल्डिंग में एक मेज पर बैठे विश्लेषकों ने कुछ और भी देखा, 6 एसएस4 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर तक मार करने में सक्षम थीं. नेशनल फोटो इंटरप्रिटेशन सेंटर के चीफ आर्थर लुंडाहल ने अपने स्टाफ से कहा, ‘हम अपने समय की सबसे बड़ी खबर को देख रहे हैं.’ चंद घंटों के भीतर ही इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया और फिर वापस लौटने में भी मदद की.
दरअसल प्रयास ये किए जा रहे हैं कि अमेरिका की अगुवाई वाले ‘फाइव आईज’ क्लब में भारत को भी शामिल किया जाए. ‘फाइव आईज’ को मानवीय इतिहास में सबसे कुशल खुफिया जानकारी जुटाने वाले अलाएंस के तौर पर देखा जाता है. अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस पर संसद की आर्म्ड सर्विसेज सबकमिटी के चेयरमैन सीनेटर रूबेन गलिगो ने 2022 के लिए रक्षा विधेयक पर बात करते हुए नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर से फाइव आईज क्लब को समान विचारों वाले लोकतांत्रिक देशों के लिए खोलने से जुड़े फायदे और नुकसान पर रिपोर्ट करने को कहा है.
इसका मतलब है कि फाइव आईज क्लब में जापान, दक्षिण कोरिया और भारत को भी शामिल किया जा सकता है, साथ ही उन यूरोपीय देशों को भी शामिल किया जा सकता है, जोकि चीन के खिलाफ आसन्न शीत युद्ध में विश्वास करते हैं. भारत और अमेरिका 2015 से ही अपनी इंटेलिजेंस रिलेशनशिप को मजबूत बनाने पर लगातार बात कर रहे हैं. इसमें एक तरह से फाइव आईज क्लब में भारत को शामिल किए जाने पर भी चर्चा होती रही है. ऐसे में अमेरिकी रक्षा विधेयक की भाषा बताती है कि इस विचार को गति मिल रही है.
सैद्धांतिक रूप से फाइव आईज की सदस्यता भारत के लिए चीन के खिलाफ काफी मददगार साबित होगी. चीन के रणनीतिक कम्युनिकेशन को भेद पाना और जानकारी जुटा पाना, साथ ही लैंग्वेज और क्षेत्रीय विशेषज्ञों का पूल बना पाने के मामले में भारत हमेशा से संघर्ष करता रहा है. हालांकि सभी समझौतों की तरह फाइव आईज क्लब की सदस्यता भी अपने साथ नियम और शर्तें लेकर आती है. इनमें से काफी शर्तें आकर्षक भी नहीं होती हैं.
फाइव आइज़ की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान के लिए हुई थी. 1955 में इसे औपचारिक गठबंधन के तहत विस्तार दिया गया और अंग्रेजी बोलने वाले लोकतांत्रिक देशों को शामिल किया गया. इसके तहत पांच देशों द्वारा दुनिया भर में श्रवण केंद्र चलाए जा रहे हैं. 1970 के दशक में इन केंद्रों को सैटेलाइट्स से भी मदद मिली और एक तरीके से इन्हें धरती पर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सुनने की अनुमति भी मिल गई.
1990 के दशक में फाइव आइज का ऑपरेशन सार्वजनिक होता गया. दरअसल न्यूजीलैंड के निकी हेजर, अमेरिका के जेम्स बम्फोर्ड और ब्रिटेन के पत्रकार डंकन कैंपबेल ने इस बारे में खुलासे किए. रिपोर्ट्स पब्लिक होने के बाद लोगों में इस बात की आशंका बढ़ गई कि सदस्य देश अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी को अंजाम दे सकते हैं, साथ ही इसका इस्तेमाल वे अपने व्यापारिक हित के लिए भी कर सकते हैं.
साल 2000 और 2001 में यूरोपीय संसद ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए बताया कि लोगों की आशंका सही थी. इसके बाद मचे हंगामे ने अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर जेम्स वूल्सी को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया कि अमेरिका ने यूरोप में जासूसी को अंजाम दिया. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को टारगेट किया और समझौते हासिल करने के लिए रिश्वत भी दी. हालांकि उन्होंने दावा किया कमर्शियल और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का उपयोग अमेरिका में मौजूद कंपनियों के खिलाफ नहीं किया गया.
बाद में कनाडा के इंटेलिजेंस ऑफिसर फ्रेड स्टॉक के बयानों से भी वूल्सी के दावों की पुष्टि हुई और पाया गया कि वूल्सी ने सच कबूला था. स्टॉक को 1993 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, उनका दावा था कि उन्होंने इकोनॉमिक और सिविलियंस को टारगेट करने का विरोध किया था. स्टॉक के मुताबिक अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, चीन द्वारा अनाजों की खरीद और फ्रांस द्वारा हथियारों की बिक्री पर भी इंटेलिजेंस के द्वारा नजर रखी थी. फाइव आइज के ऑपरेशंस के बारे में अमेरिका के पूर्व एनएसए ऑफिसर एडवर्ड स्नोडेन ने भी 2013 में खुलासा किया था. स्नोडेन ने कहा था कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के द्वारा अमेरिकी नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया.
अगर प्राइवेसी के मुद्दे को छोड़ दें तो फाइव आइज की सदस्यता के फायदे इसके खतरों के मुकाबले कुछ भी नहीं हैं. सर्विलांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग सप्लायर्स पर निगाह रखने के लिए की जा सकती है. दशकों तक भारत, पाकिस्तान और ईरान जैसे देश स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रिप्टोएजी से इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एक्विपमेंट खरीदते रहे हैं. लेकिन, 2015 में एनएसए के दस्तावेजों से पता चला कि क्रिप्टोएजी का मालिकाना गुप्त रूप से सीआईए और जर्मनी की बीएनडी के पास है, जो इन्क्रिप्शन एल्गोरिथम को इस तरह डिजाइन करती थीं कि उनकी इंटेलिजेंस सर्विसज दूसरे देशों की बातचीत को पूरी तरह सुन सकें.
ईरान में 1979 की क्रांति के समय अयतुल्लाह खेमनई पर निगाह रखने के लिए सीआईए ने इसका उपयोग किया था. बाद में अर्जेंटीना के मिलिट्री कम्युनिकेशन की जानकारी अमेरिका ने फॉकलैंड्स युद्ध के समय ब्रिटेन को दी. अमेरिका ने ही इस बात का पता लगाया कि बर्लिन में हुए आतंकी हमलों के लिए लीबिया जिम्मेदार है. इसका पता उन्होंने सबूतों के साथ लगाया. माना जाता है कि अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के इंटेलिसजेंस कम्युनिकेशन को भी सुनता है. हालांकि उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि दोनों देशों के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भनक अमेरिका को नहीं थी. अमेरिका 1962 से ही चीन पर नजर रख रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि अमेरिका किस हद तक चीन की जासूसी में कामयाब रहा है.
फाइव आइज के सदस्य देश, जैसेकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और उनका मानना है कि अपनी निजता की बिनाह पर उन्हें संकट के समय फाइव आइज से काफी मदद मिली है. हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली और टोक्यो किसी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन कोई भी फैसला बेहद समझदारी से लिया जाना चाहिए. फाइव आइज के साथ एक और समस्या ये है कि ये बहुत ज्यादा तकनीक पर निर्भर है. अमेरिका इंटेलिजेंस बजट का 70 फीसदी उपकरणों पर खर्च करता है. लेकिन सोवियत यूनियन ने परंपरागत जासूसी के तरीकों से ज्यादा कामयाबी पाई है. इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि रूस ने अमेरिकी न्यूक्लियर प्रोग्राम के केंद्र में अपना जासूस बिठा दिया था. साथ ही कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस के लिए भी उसने अपने जासूस फिट कर रखे थे.
एक बहुत फेमस केस में सीआईए ने बर्लिन के अंदर एक टनल का इस्तेमाल सोवियत संघ के फोन कम्युनिकेशन को सुनने के लिए शुरू किया. ये किस्सा 1953 का है. लेकिन इस टनल में सोवियत संघ ने ब्रिटेन के डबल एजेंट जॉर्ज ब्लेक के जरिए सेंध लगा दी और भ्रामक संदेशों के जरिए अपने विरोधियों को उलझाए रखा. क्यूबा में सोवियत संघ की मिसाइलों को पकड़े जाने की U2 तस्वीर भी इसलिए हासिल हो पाई क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस को मास्को में तैनात मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ओलेग पेन्कोवस्की ने जानकारी दी थी. अगर जानकारी नहीं होती तो फोटो इंटरप्रिटेशन एक्सपर्ट मास्को के करीब फैसिलिटीज सेंटर को पहचान भी नहीं पाते.
हालांकि सबक ये नहीं है कि तकनीक कारगर नहीं है, बल्कि सबक ये है कि तकनीक की एक सीमा है. 2019-20 में भारत सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 2,575 करोड़ का बजट रखा था. ये राशि दिल्ली पुलिस को आवंटित की गई 7,497 करोड़ की राशि से भी कम है. भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थिति को देखें तो पश्चिमी देशों के मुकाबले यह कहीं नहीं ठहरती. 2020 के लिए एफबीआई का बजट 9.6 बिलियन डॉलर का है.
2013 में संसद को बताया गया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में कम से कम 8 हजार पद खाली है. हालांकि स्थितियों में उसके बाद से ज्यादा बदलाव नहीं आया है. विशेषज्ञ इस बात को समझते हैं और समय-समय पर बदलाव की मांग करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बारे में कह चुके हैं. लेकिन अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है.