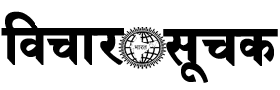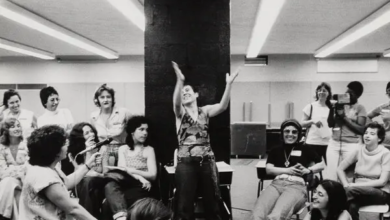भारतीय बैंकिग को अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत

प्रेम शर्मा
पिछले लम्बे अरसे से भारतीय बैंकिंग व्यवस्था सुधार की कवायद की जा रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कई बैंको के विलय के बावजूद बैंकिंग सेक्टर में अपेक्षित सुधार नही आ पाया अब लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस में विलय को लेकर भी सवाल खड़े हो गए है। बैंकिंग ढांचे में सुधार के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक की एक समिति ने यह जो कहा कि कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग कंपनियों में प्रमोटर बनने का अवसर मिलना चाहिए वह एक सही सुझाव प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह भी देखने की आवश्यकता है कि बैंकिंग क्षेत्र में कहीं अधिक सुधारों की जरूरत है। इससे भी अधिक इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब तक सुधार के कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आते तब तक बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिष्ठा को स्थापित करना मुश्किल होगा। इससे इन्कार नहीं कि पिछले कुछ वर्षो में रिजर्व बैंक ने बैंकों में सुधार को गति देने वाले एक के बाद एक कदम उठाए हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गड़बडिय़ों और विसंगतियों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
बैंकिंग ढांचे में कोई बड़ी गड़बड़ी सामने आती है तो न केवल बैंक प्रबंधन पर सवाल उठते हैं, बल्कि ऐसे मामलों पर रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार की भूमिका पर भी बहस आरंभ हो जाती है। पिछले दिनों लक्ष्मी विलास बैंक के खाताधारकों पर यह शर्त लगाई गई कि वे 25,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते। ऐसा इसलिए करना पड़ा, क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। इसके पहले भी कुछ अन्य बैंकों के खाताधारकों को लगभग ऐसी ही परिस्थितियों में इस प्रकार की शर्तो से दो चार होना पड़ा है। बैंकिंग ढांचे में सुधार के कदमों को आगे बढ़ाने के साथ ही इस पर भी विचार करना चाहिए कि उनके फंसे हुए कर्जो पर उल्लेखनीय कमी कैसे आए। फंसे हुए कर्जों को एक सीमा तक नियंत्रित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस चुनौती का एक बड़ा कारण बैंकिंग क्षेत्र के मामले में नीर-क्षीर निर्णय लेने में ढिलाई और राजनीतिक लाभ-हानि को अधिक महत्व देना भी है। यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के फंसे हुए कर्जो की समस्या सतह पर आने के बाद सुधार के प्रयास तेज हुए हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसको लेकर हर स्तर पर सजगता बरती जा रही है।
जहां तक बड़े बैंकों की जरूरत रेखांकित करने की बात है तो यह बहुत पहले से कहा जा रहा है कि बैंकों की तादाद की उतनी जरूरत नहीं जितना कि उनका बड़ा और सक्षम होना। ऐसे में रिजर्व बैंक की समिति की सिफारिशों पर अमल के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बैंक उन खामियों से मुक्त हों जिनके चलते वे रह-रहकर संकट से घिर जाते हैं और भरोसे का संकट उत्पन्न हो जाता है। वर्ष 2014 से राजग सरकार की बैंकिंग नियमों को देखें तो साफ हो जाता है कि इसके कार्यकाल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में विलय कर उन्हें एक मजबूत बैंक बनाने के लिए लगातार फैसले हुए हैं। सितंबर, 2019 में सरकारी क्षेत्र के 10 बैंकों को मिला कर चार बैंकों में तब्दील करने का फैसला किया है। अप्रैल, 2020 से विलय प्रक्रिया लागू की गई है। इसके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक व विजया बैंक के विलय और एसबीआइ में इसके सभी सब्सिडियरी बैंकों को मिलाने का फैसला भी राजग सरकार के कार्यकाल में किया गया था। इसी बीच सरकारी क्षेत्र के आईडीबीआइ बैंक में सरकार ने अपनी अहम हिस्सेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम को बेच दी थी। अब आइडीबीआइ बैंक में सरकार अपनी मौजूदा 47 फीसद हिस्सेदारी भी घटाने का रास्ता तलाश रही है। निजी क्षेत्र के कर्जदाता लक्ष्मी विलास बैंक और सिंगापुर स्थित डीबीएस होल्डिंग्स की भारतीय शाखा के विलय में बैंकिंग क्षेत्र के संगठनों को गड़बड़झाला लग रहा है।
बैंक के शेयरधारकों, आम नागरिकों और कई बैंकिंग यूनियन का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने जिस तरह से डीबीएस इंडिया को लक्ष्मी विलास बैंक मुफ्त में देने का फैसला किया है, उसमें कई झोल हो सकते हैं। ऑल इंडिया बैंक इंप्लॉईज एसोसिएशन (एआइबीईए) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि आरबीआइ के नेतृत्व में एलवीबी के डीबीएस इंडिया में विलय की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें बड़ा झोल नजर आ रहा है। आरबीआइ इस विलय को लेकर जिस जल्दबाजी में दिख रहा है, उसमें घोटाले की आशंका भी दिखाई दे रही है। बैंक के एक लाख से अधिक शेयरधारकों को विलय योजना पर प्रतिक्रिया देने के लिए महज तीन दिनों का वक्त दिया गया है। एलवीबी का ठीक से मूल्यांकन तक नहीं किया गया है। आरबीआइ ने मंगलवार को कहा कि विलय के अस्तित्व में आने के बाद एलवीबी का परिचालन बंद समझा जाएगा। बैंक के शेयर और डिबेंचर डिलिस्ट माने जाएंगे, यानी किसी भी शेयर बाजार में उनकी खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी। ऐसे में यह बुनियादी सवाल यह है कि एलवीबी को संपदा बिक्री की प्रक्रिया से क्यों नहीं गुजारा गया और डिजॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआइसीजीसी) को सामने आने तथा बैंक को पूंजी मुहैया कराने का मौका क्यों नहीं दिया गया।
अगर डीआइसीजीसी को पूंजी मुहैया कराने दिया जाता, तो जमाकर्ताओं को निकासी की सुविधा मिल सकती थी। अगर किसी बैंक के विफल होने की चुभन उसमें शामिल सभी पक्षों तक नहीं पहुंचेगी, तो बैंकों का इस तरह विफल होना जारी रहेगा। वैसे इस बॉत को नकारा नही जा सकता कि देश की बढ़ती इकोनॉमी के हिसाब से विशाल आकार के बैंक स्थापित करने के लिए सरकार की कोशिशों को आरबीआइ कार्यदल के सुझावों से मदद मिलेगी। इसके आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों के निजीकरण को लेकर भी आगे बढ़ सकती है।आरबीआइ के आंतरिक कार्यदल ने बैंकों की होल्डिंग पैटर्न (मालिकाना हक संबंधी हिस्सेदारी) में बदलाव को लेकर जो सिफारिशें की है वह केंद्र सरकार के वृहत बैंकिंग सुधार का ही हिस्सा है। केंद्र सरकार पहले से ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बड़े बदलाव के एजेंडे पर काम कर रही है। वैसे भी हाल के दिनों में श्रम कानूनों व कृषि क्षेत्र में कई वर्षो से अटके सुधारों पर दो टूक फैसला करने के बाद केंद्र सरकार अब बैंकिंग सुधारों पर फैसला करने जा रही है। आरबीआइ के कार्यदल की सिफारिशों में भारत में बड़े व व्यापक पूंजी आधार वाले बैंकों की जरूरत पर खास तौर पर जोर दिया गया है।वित्त मंत्रालय में इस बारे में लगातार विमर्श चल रहा है। वित्त मंत्रालय की दूसरे संबंधित मंत्रालयों व नियामक एजेंसियों से भी बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधारों का समर्थक है।
निजी क्षेत्र के मौजूदा बैंकों को बड़े पैमाने पर विस्तार करने और बड़े औद्योगिक घरानों को बैंकिंग सेक्टर में उतरने की इजाजत देना इस एजेंडे का अहम हिस्सा होगा। अभी सार्वजनिक क्षेत्र के तीन ऐसे बैंक है जिनमें सरकार अपनी इक्विटी बेचने को इच्छुक है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब व सिंध बैंक और यूको बैंक हैं। आईडीबीआइ बैंक में भी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच कर बाहर निकलना चाहती है। इन चारों बैंकों के बारे में जल्द ही बड़े अहम अहम फैसला किये जाने के आसार हैं। ऐसे में भारत के बड़े औद्योगिकी घरानों को भी बैंकिंग सेक्टर में उतरने में ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में मौजूदा नियमों में कई तरह के संशोधन की सिफारिश की गई है। इस बारे में तर्क देते हुए यह रिपोर्ट कहती है कि, दिसंबर, 2019 तक दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों में भारत का एकमात्र बैंक एसबीआइ है। इस सूची में सौवें स्थान पर स्पेन का बैंका दी साबादेल है जिसका पूंजी आधार 18 लाख करोड़ रुपये का है। जबकि एसबीआइ के बाद भारत के चारों बड़े बैंकों का पूंजी आधार बैंका दी साबादेल से बहुत ही कम है। यानि कि देश के बैंकिग सेक्टर को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।